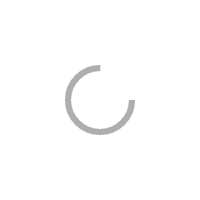सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून के दायरे पर एक अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल में सदस्यता लेना या उसमें सक्रिय रूप से जुड़ना “रोजगार” की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए, इस तरह की परिस्थितियों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Prevention of Sexual Harassment at Workplace – POSH) अधिनियम, 2013 स्वतः लागू नहीं होगा। अदालत ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस कानून का मनमाना इस्तेमाल ब्लैकमेल और दुरुपयोग का जरिया बन सकता है।
पॉश अधिनियम का मामला क्या था
यह विवाद केरल में एक महिला द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा था। महिला ने दावा किया था कि वह एक राजनीतिक दल की सक्रिय कार्यकर्ता थीं और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। महिला ने इस मामले को पॉश अधिनियम के तहत उठाया और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन की मांग की। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी कि राजनीतिक दल की सदस्यता रोजगार संबंध नहीं बनाती।
महिला ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि पॉश अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचाना है, चाहे वे वेतनभोगी हों या स्वेच्छा से किसी संगठन में काम कर रही हों। वकील ने तर्क दिया कि “पीड़ित” की परिभाषा केवल वेतन या औपचारिक नियुक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि पॉश अधिनियम का मूल उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है। लेकिन किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना या सिर्फ सदस्य होना रोजगार की परिभाषा में नहीं आता।
पीठ ने कहा, “अगर हम राजनीतिक दल में शामिल होने या चुनावी अभियान में सक्रिय रहने को रोजगार मान लें, तो यह कानून के मूल मकसद को विकृत कर देगा। ऐसा करने से यह अधिनियम ब्लैकमेल और दुरुपयोग का जरिया बन सकता है।” अदालत ने कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल न केवल निर्दोष लोगों को परेशान करेगा, बल्कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी कमजोर करेगा।
पॉश अधिनियम का उद्देश्य और दायरा
2013 में लागू हुआ पॉश अधिनियम भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून हर उस संगठन पर लागू होता है जहां कर्मचारी, इंटर्न, प्रशिक्षु या वेतनभोगी कार्यरत हैं।
कानून के तहत: पॉश अधिनियम
प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
शिकायत मिलने के बाद समयबद्ध तरीके से जांच और कार्रवाई का प्रावधान है।
अस्थायी, स्थायी, संविदा या प्रशिक्षु जैसे सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि “सदस्यता” और “रोजगार” के बीच अंतर है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन में जुड़ता है, तो वह रोजगार का संबंध नहीं बनाता।
पीड़ित की परिभाषा पर बहस
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने दलील दी कि “पीड़ित” शब्द का अर्थ सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि कई महिलाएं राजनीतिक दलों या गैर-लाभकारी संगठनों में बिना वेतन के काम करती हैं और उन्हें भी कार्यस्थल जैसा वातावरण चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद “कार्यस्थल” की स्पष्ट परिभाषा में सुरक्षा देना है, और यह परिभाषा रोजगार संबंध से जुड़ी है।
पीठ ने कहा कि अगर “पीड़ित” की परिभाषा को बिना किसी सीमा के बढ़ाया गया तो यह कानून अनियंत्रित हो जाएगा। इसका दुरुपयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन या समूह को परेशान कर सकता है।
राजनीतिक दलों के लिए संदेश
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा तेज हो गई है। भले ही पॉश अधिनियम सीधे लागू न हो, लेकिन दलों पर नैतिक जिम्मेदारी जरूर है कि वे अपनी महिला सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और संगठन में पारदर्शिता बनी रहेगी। कई दल पहले से आचार संहिता और अनुशासनात्मक समितियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें और सख्ती से लागू करने की जरूरत है।
समाज और महिला अधिकारों पर असर
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और चिंता—दोनों ही भावों के साथ किया। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह फैसला पॉश अधिनियम के मूल मकसद को स्पष्ट करता है और अनावश्यक मुकदमों को रोकने में मदद करेगा। वहीं, कुछ ने चिंता जताई कि इससे कई महिलाएं जो संगठनों में बिना वेतन के काम करती हैं, उनके पास कानूनी सुरक्षा के कम विकल्प रह जाएंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना केवल कानून का नहीं, बल्कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। राजनीतिक दलों, गैर-लाभकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने स्तर पर आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा मिले।
पॉश अधिनियम के आगे का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पॉश अधिनियम की सीमाओं को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि कानून का दायरा कहां तक है। हालांकि, इस फैसले से यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या भविष्य में ऐसे संगठनों के लिए अलग कानून की आवश्यकता होगी जहां लोग बिना वेतन के काम करते हैं लेकिन वहां यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो सकती हैं।
कानूनी जानकार मानते हैं कि सरकार चाहे तो इस दिशा में पहल कर सकती है। स्वयंसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल और सामाजिक समूह ऐसे स्थान हैं जहां महिलाएं बड़ी संख्या में सक्रिय होती हैं। उनके लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान बनाना समय की मांग हो सकता है।
यह भी पढ़ें – शाहिद अफरीदी की राहुल गांधी पर तारीफ और मोदी सरकार पर हमला, भारत में गरमाई सियासत